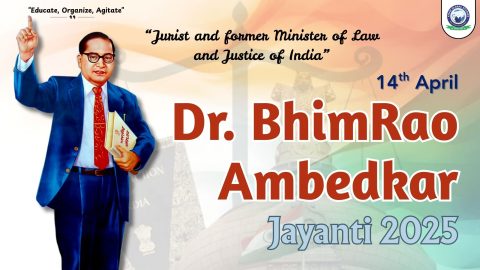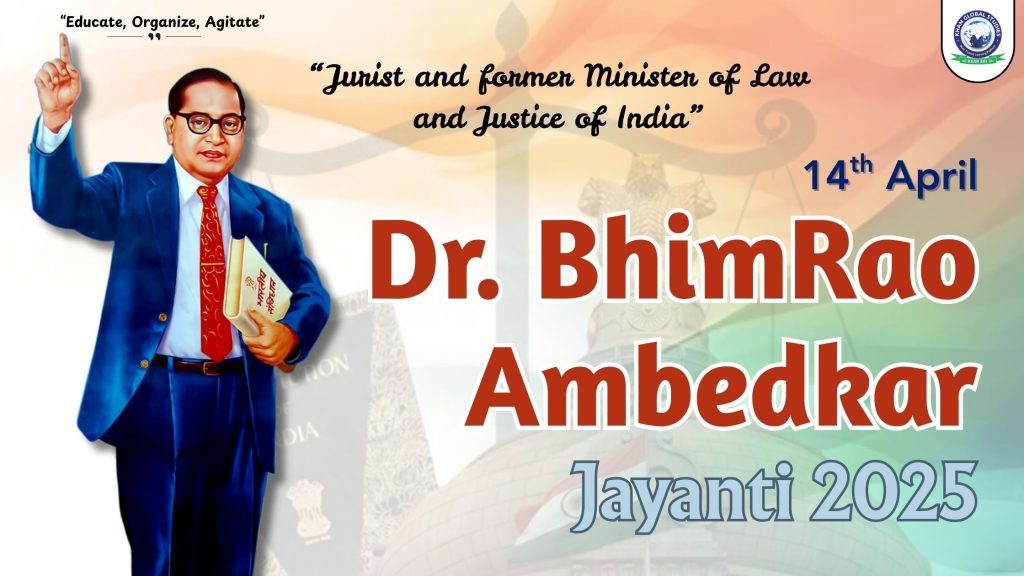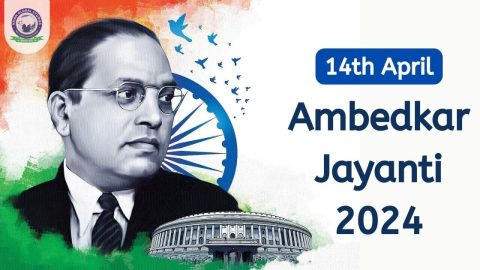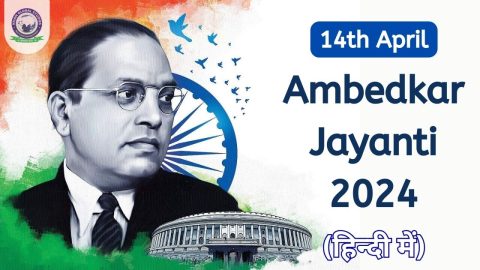डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्यप्रदेश के महू छावनी क्षेत्र में हुआ था। वे महार जाति से संबंध रखते थे, जिसे उस समय समाज में अस्पृश्य माना जाता था। उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे, जिनसे उन्हें अनुशासन, ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता की प्रेरणा मिली। बचपन से ही उन्हें जातिगत भेदभाव और सामाजिक उपेक्षा का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी।
प्रारंभिक शिक्षा और संघर्ष
डॉ. भीमराव अंबेडकर ने सतारा और मुंबई जैसे शहरों में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। स्कूल में उन्हें अक्सर जमीन पर बैठाया जाता था और उन्हें पानी पीने तक से वंचित कर दिया जाता था। इसके बावजूद उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया। एलफिंस्टन कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश पाकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि ज्ञान सामाजिक सीमाओं से ऊपर होता है। उनके लिए शिक्षा केवल आत्म-विकास नहीं, बल्कि समाज के उत्थान का साधन थी।
विदेश यात्रा और उच्च शिक्षा
1913 में उन्हें बड़ौदा राज्य के गायकवाड़ महाराजा से छात्रवृत्ति मिली, जिसके माध्यम से वे अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय गए। वहाँ उन्होंने अर्थशास्त्र में M.A. और Ph.D. की उपाधियाँ प्राप्त कीं। इसके बाद वे लंदन गए और वहाँ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से D.Sc. किया तथा कानून की पढ़ाई पूरी कर ‘बार-एट-लॉ’ बने। उनकी शैक्षणिक उपलब्धियाँ न केवल व्यक्तिगत गौरव का विषय थीं, बल्कि पूरे भारत के लिए प्रेरणास्रोत बनीं।
सामाजिक संघर्ष और आंदोलन
विदेश से लौटने के बाद अंबेडकर ने समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग के लिए कार्य आरंभ किया। उन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1927 में चवदार तालाब सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने दलितों को सार्वजनिक जलस्रोतों तक पहुँच का अधिकार दिलाया। 1930 में कालाराम मंदिर सत्याग्रह द्वारा धार्मिक स्थलों में समान प्रवेश की माँग की। ये सभी आंदोलन सामाजिक समानता की दिशा में मील का पत्थर साबित हुए।
राजनीतिक सक्रियता
डॉ. अंबेडकर का मानना था कि सामाजिक परिवर्तन के लिए राजनीतिक शक्ति आवश्यक है। 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की और 1937 में बॉम्बे विधानसभा के सदस्य चुने गए। उन्होंने दलितों के राजनीतिक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। आगे चलकर उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की, जो सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए एक संगठित मंच बना।
संविधान निर्माण में अमूल्य योगदान
भारत की आज़ादी के बाद 1947 में उन्हें संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया, जिसे 26 नवम्बर 1949 को अंगीकृत किया गया। इस संविधान में समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों की स्थापना की गई। डॉ. अंबेडकर का उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना था जहाँ हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार हो।
धर्म परिवर्तन और बौद्ध धर्म की ओर रुझान
डॉ. अंबेडकर ने हिंदू धर्म की जातिगत व्यवस्था से निराश होकर 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उन्होंने घोषणा की, “मैं हिंदू जन्मा हूँ, पर हिंदू के रूप में मरूँगा नहीं।” उनके साथ लाखों अनुयायियों ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया। यह केवल एक धार्मिक परिवर्तन नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक क्रांति थी।
लेखन और बौद्धिक योगदान
डॉ. अंबेडकर एक गहन चिंतक और प्रखर लेखक थे। उनकी प्रमुख रचनाओं में “Annihilation of Caste”, “Who Were the Shudras?” और “The Buddha and His Dhamma” शामिल हैं। उन्होंने संविधान, समाज, धर्म और अर्थशास्त्र पर व्यापक लेखन किया। उनके विचार आज भी सामाजिक सुधार और समानता की दिशा में प्रेरणा प्रदान करते हैं।
समान नागरिक संहिता
डॉ. भीमराव अंबेडकर न केवल सामाजिक समानता के प्रबल समर्थक थे, बल्कि वे भारत में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को लागू करने के पक्ष में भी दृढ़ता से खड़े थे। वे मानते थे कि एक आधुनिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले भारत में पर्सनल लॉ की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। संविधान सभा की बहसों के दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से भारतीय समाज में सुधार लाने के लिए समान नागरिक संहिता को अपनाने की जोरदार सिफारिश की थी।
चुनावी पराजय और राज्यसभा सदस्यता
1952 के लोकसभा चुनाव में डॉ. अंबेडकर ने बॉम्बे (उत्तर-मध्य) निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन वे पराजित हो गए। उन्हें 1,23,576 मत मिले जबकि कांग्रेस प्रत्याशी नारायण सडोबा काजोलकर को 1,38,137 मत प्राप्त हुए। इसके पश्चात् मार्च 1952 में उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया, और वे अपने जीवन के अंतिम समय तक इस सदन में सेवा करते रहे।
अर्थशास्त्र में योगदान और आर्थिक दृष्टिकोण
डॉ. अंबेडकर विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। उनका मानना था कि भारत की आर्थिक प्रगति का मार्ग औद्योगिकीकरण और कृषि सुधारों से होकर गुजरता है। उन्होंने कृषि को प्राथमिक उद्योग मानते हुए इसमें निवेश की आवश्यकता पर बल दिया। शरद पवार के अनुसार, अंबेडकर के दृष्टिकोण ने भारत को खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
वे शिक्षा, सार्वजनिक स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं और आवास को राष्ट्रीय विकास के मूल आधार मानते थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के आर्थिक दुष्प्रभावों का गहराई से विश्लेषण करते हुए भारत की आत्मनिर्भरता के लिए ठोस योजनाएँ प्रस्तुत कीं।
भारतीय रिज़र्व बैंक और अर्थशास्त्र पर लेखन
डॉ. भीमराव अंबेडकर न केवल एक समाजशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे, बल्कि एक कुशल अर्थशास्त्री भी थे। 1921 तक वे एक पेशेवर अर्थशास्त्री के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। उनकी तीन प्रमुख कृतियाँ—
- Administration and Finance of the East India Company
- The Evolution of Provincial Finance in British India
- The Problem of the Rupee: Its Origin and Its Solution
—अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनके गहन ज्ञान को दर्शाती हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन को उनके दिए गए सुझावों के आधार पर हुई थी, जो इस बात का प्रमाण है कि उनकी सोच कितनी दूरदर्शी और ठोस थी।
नारी सशक्तिकरण में अग्रणी भूमिका
डॉ. अंबेडकर को भारत का एक महान नारीवादी चिंतक भी माना जाता है। उन्होंने अपने लेखन और कार्यों के माध्यम से महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के निरंतर प्रयास किए। उनका मानना था कि मनु से पूर्व भारतीय समाज में महिलाओं को सम्मान, शिक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी, किंतु मनुस्मृति ने महिलाओं की स्थिति को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त किया।
डॉ. अंबेडकर ने ‘मूकनायक’ और ‘बहिष्कृत भारत’ जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। 1941 में जब सरकार ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण की पहल की, तो डॉ. अंबेडकर ने कानून मंत्री के रूप में इस कार्य को अपनी ज़िम्मेदारी के रूप में लिया। हालांकि उन्हें कट्टरपंथी ताक़तों का विरोध झेलना पड़ा, फिर भी उन्होंने महिलाओं को समान अधिकार दिलाने की लड़ाई कभी नहीं छोड़ी।
निधन और स्मृति
डॉ. अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ। उनके निधन से भारत ने एक महान विचारक, समाज सुधारक और राष्ट्र निर्माता को खो दिया। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज उनके नाम पर अनेक स्मारक, संस्थान और शोध केंद्र स्थापित हैं जो उनके विचारों को जीवित रखते हैं।
निष्कर्ष
डॉ. भीमराव अंबेडकर की सोच केवल सामाजिक सुधार तक सीमित नहीं थी; वे आर्थिक नियोजन, विधिक अधिकारों और महिला सशक्तिकरण के भी सजग प्रवर्तक थे। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और एक समतामूलक, वैज्ञानिक और न्यायपूर्ण भारत के निर्माण की दिशा में प्रेरणा देते हैं।
डॉ. भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष, शिक्षा, न्याय और सामाजिक समरसता की मिसाल है। उन्होंने न केवल अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष किया, बल्कि भारत को एक ऐसा संविधान भी दिया जो हर नागरिक को समान अधिकार और सम्मान प्रदान करता है। उनका संदेश – “शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो” – आज भी समाज के हर वर्ग के लिए एक मार्गदर्शक है। वे न केवल दलित समाज के, बल्कि पूरे राष्ट्र के गौरव हैं।